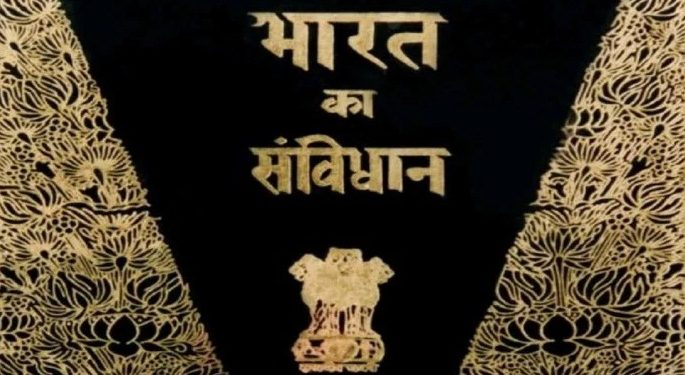प्रकाश मेहरा
एक्जीक्यूटिव एडिटर
देहरादून। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां आजीविका, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि की उपलब्धता बहुत ही कम है। खेती अलाभकारी है। श्रम का मूल्य अत्यल्प होने से परिवार का भरण-पोषण करना दुष्कर हो गया है। ऐसे ही अनेक कारणों से लोग अपने पूर्वजों की भूमि को त्याग कर अन्यत्र बसते जा रहे हैं।
यही कारण है कि तमाम हिमालयी राज्यों में अकेला उत्तराखंड ही है जहां राज्य सरकार द्वारा पलायन की समस्या की गहराई से जांच करने और इसका समाधान खोजने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और पलायन रोकने के लिए ठोस नीति बनाना है।
हालांकि, कुछ अन्य हिमालयी राज्यों ने भी पलायन और जनसांख्यिकी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी संरचना और उद्देश्य अलग हैं।
1. हिमाचल प्रदेश—इस राज्य में पलायन की समस्या को समझने और रोकने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन कोई विशेष ‘पलायन आयोग’ नहीं है। राज्य की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुधारने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित रहती हैं।
2. जम्मू और कश्मीर—यहां पलायन की समस्या मुख्य रूप से राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से हुई है। राज्य सरकार ने कश्मीरी पंडितों और अन्य प्रवासी समुदायों की समस्याओं को समझने के लिए अलग-अलग समितियां और आयोग बनाए हैं। हालांकि, ये आयोग पलायन की व्यापक समस्या से नहीं, बल्कि विशिष्ट समूहों की समस्याओं से जुड़े हैं।
3. सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश—इन राज्यों में पलायन की समस्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन जनजातीय समुदायों के विकास और आजीविका के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।
जिस प्रकार लाहौल और स्पीति को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने से वहाँ शिक्षा सेवाओं में सुधार हुआ और वहीं आरक्षण मिलने से देश व प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए युवाओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। लोगों के जीवनस्तर में सुधार हुआ है।
ऐसे अनेक कारणों से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को भी संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने के अपरिमित लाभ यहाँ के लोगों को मिलने से पलायन की समस्या का किसी हद तक समाधान हो सकता है।