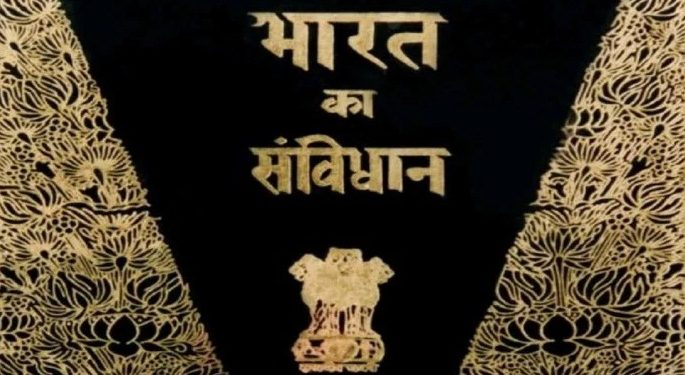कौशल किशोर
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद और पंथनिरपेक्षता पर लंबित मुकदमा खारिज कर दिया है। संविधान दिवस मनाने के ठीक पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे राजनीतिक जुमले भारतीय संदर्भ सहित परिभाषित हुई है।
सुब्रमण्यम स्वामी, बलराम सिंह और अश्विनी कुमार उपाध्याय जैसे पक्षकारों की बात सुनी गई। उन्हें इससे संतोष करना होगा। साथ ही आपातकाल में इन्दिरा गांधी की तानाशाही के सामने तन कर खड़े होने का साहस दिखाने वाले जस्टिस एच.आर. खन्ना को याद करना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का यह फैसला मुकदमा खारिज होने के बावजूद भी ऐतिहासिक महत्व का है।
संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद व पंथनिरपेक्ष शब्द 2 नवंबर 1976 को आपातकाल में हुए 42वें संशोधन के कारण जोड़ा गया था। निश्चय ही स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चलने वाला आपातकाल ही है। इसी दौरान भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान करने वाले संविधान में कर्त्तव्य भी जोड़े गए थे। दरअसल मार्च 1971 में गठित हुई पांचवीं लोक सभा का कार्यकाल मार्च 1976 में समाप्त होना चाहिए।
याचिका दायर करने वाले इस संशोधन को इस कारण से खारिज करने की मांग करते। हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 1978 में 44वें संशोधन में इसे बदलना जरूरी नहीं माना गया था। आज सर्वोच्च न्यायालय भी इसे वैध करार देती है। भारतीय संदर्भ में दोनों ही शब्दों को परिभाषित करती है। इसमें ‘समाजवाद’ शब्द आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लक्ष्यों को दर्शाता है। इसके लिए ‘वेलफेयर स्टेट’ शब्द को पर्याय माना गया।
व्यापार और वाणिज्य को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख कर संविधान नागरिकों की निजी उद्यमशीलता को प्रतिबंधित नहीं करती है। यहां ‘पंथनिरपेक्ष’ का अर्थ धर्मविरुद्ध होना कतई नहीं है। यह समानता के नागरिक अधिकार को प्रदर्शित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक योजना को दर्शाने वाले मूल ताने-बाने में बुना हुआ माना है।
संविधान सभा के 299 सदस्यों ने मिल कर 2 साल 11 महीने और 17 दिनों का समय लगाया और लोकतंत्र की सर्वोच्च संहिता रचने का काम किया था। इसकी गतिशीलता बनी रहे, इसलिए संशोधन का मार्ग भी प्रशस्त किया। फलत: समय के साथ ताल मिलाने के क्रम में अब तक 106 संशोधन किए गए हैं। इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। न्याय दिवस के रुप में इसे मनाने का रिवाज 2014 तक चलता रहा। लेकिन मोदी सरकार 2015 में इसे संविधान दिवस के रुप में मनाना शुरू करती है। संवैधानिक मूल्यों को लेकर सरकार अपनी प्रतिबद्धता तभी से लगातार दोहरा भी खूब रही है। विपक्ष की राजनीति इसे संविधान बदलने के नाम पर प्रचारित करती है। यहां अलग किस्म का विवाद खड़ा होता दिखता है।
संविधान सभा की बहस में समाजवाद और सेकुलरवाद का प्रसंग भी मिलता है। उस समय इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में जगह नहीं मिली थी। कम्युनिस्ट नेता हसरत मोहानी संविधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना पर जारी बहस के दौरान भारत का नाम यूएसएसआर की तर्ज पर यूआईएसआर (यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स) का प्रस्ताव दिया था। इससे उनका आशय भारतीय समाजवादी गणराज्यों के संघ से था। उसी दिन पंथनिरपेक्षता के मुद्दे पर भी चर्चा का रिकॉर्ड है। इसे समझने के लिए प्रस्तावना में ईश्वर और गांधी का उल्लेख करने का मसला खारिज किए जाने का प्रसंग पलटना होगा।
संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। भारत के लोग और भारतीय संविधान के बीच एक ऐसा रिश्ता है, जो अपने अल्पमत पर बहुमत का शासन नहीं थोपने की पैरवी करता। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के साथ इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का विधान किया गया है। सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ ही व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने का प्रयास भी इसमें खूब सन्निहित है।
संविधान सभा में साफ कहा गया था कि सरकारें लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होंगी। मतदान की प्रक्रिया इसी का नतीजा है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र कानून के शासन द्वारा संचालित होगा। सरकार के संस्थानों और अंगों पर हुई चर्चा में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि सरकारें राज्य के दस्तावेजों से अस्तित्व में नहीं आती हैं। सही मायनों में संप्रभुता सम्पन्न स्वतंत्र भारत के संस्थानों और सरकार के अंगों को सभी शक्ति और अधिकार लोगों से ही प्राप्त होती है। इसका पुनर्पाठ आज आवश्यक है।
बीसवीं सदी में भारतीय राष्ट्र-राज्य के निर्माताओं ने लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती को स्वीकार कर संविधान के निर्माण का प्रयोग शुरु किया। इसके कारण 1928 में मोती लाल नेहरु रिपोर्ट आई थी, जिसके सचिव जवाहर लाल नेहरु रहे। दो दशक बाद आखिरकार संविधान सभा के सदस्यों के साथ मिल कर डा. आंबेडकर ने मसौदा तैयार किया था। डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में इस संविधान की प्रस्तावना पर अंतिम निर्णय लिया गया और समाजवाद तथा पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों को बाहर रख गया था। आज कोर्ट इसकी व्याख्या कर उल्लेखनीय योगदान देती है। इसके बावजूद भी संसद में इसे संशोधित करने की शक्ति निहित है।