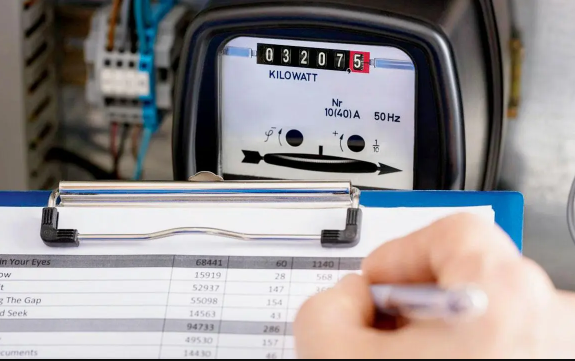एनर्जी ट्रांजिशन के एक पहलू को लक्षित करने वाले समाधान, अक्सर अन्य जलवायु और विकास लक्ष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों की अनदेखी करते हैं। यह जलवायु कार्रवाई के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण का समय है।
2015 पेरिस समझौते में, देशों को 2020 तक, अपनी दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई रणनीतियों को प्रस्तुत करने की जरूरत थी। कॉप26 में, भारत ने 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लक्ष्य की एक आश्चर्यजनक घोषणा की। इसका अर्थ है कि भारत का उद्देश्य, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना होगा। यह 2030 तक जलवायु वित्त में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रावधान पर निर्भर है। मंत्रियों ने इस बात को दोहराया है कि भारत अपने आधिकारिक जलवायु लक्ष्यों या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बिना वित्त पोषण के नहीं बढ़ाएगा।
एक प्रणाली दृष्टिकोण की जरूरत
भारत की योजना के दायरे और विवरण को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अपने ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुछ अल्पकालिक लक्ष्यों के बावजूद, घोषणा को व्यवहार में कैसे लाया जाएगा, इस बारे में कई सवाल बने हुए हैं। अपने वादों को पूरा करने के लिए, भारत और पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य सभी देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए मील का पत्थर तय करने और जलवायु वित्त अपेक्षाओं के साथ स्पष्ट ट्रांजिशन रोडमैप विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।
एक ट्रांज़िशन रोडमैप विकसित करने में, हमें क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण के बजाय प्रणाली वाली सोच पर भरोसा करना चाहिए। प्रणाली वाली सोच, प्रणाली को अलग-अलग घटकों में विभाजित करने के बजाय एक प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच के अंतर्संबंधों पर केंद्रित है। रोडमैप बनाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत मुद्दों के संयोजन से निपटने के साथ ‘सह-लाभ’, या पूरक लाभों की पहचान करने में मदद करता है।
यह ‘दो विपरीत वांछनीय स्थितियों, गुणों अथवा वस्तुओं के बीच संतुलन बनाने’ या अनजाने परिणामों को कम करने में भी मदद करता है, जो कि सुधारात्मक उपायों के बाकी हिस्सों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर ध्यान दिए बिना, प्रणाली के एक घटक में मौजूद मुद्दों से निपटने की कोशिश से उत्पन्न हो सकता है।
भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के साथ समस्या
कॉप26 में, भारत ने प्रतिज्ञा की कि 2030 तक उसकी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से होगा, साथ ही नेट-जीरो लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। चूंकि भूमि अधिग्रहण, पहले से ही सौर या पवन पार्क जैसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है, हमें आशंका है कि अगर भारत अधिक क्षमता विकसित करने का प्रयास करता है तो यह समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, हम सौर खेतों और चरागाहों या कृषि भूमि के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं, जो पहले से ही उपज में ठहराव और भूमि क्षरण का सामना कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट जैसे समाधान, पहले से ही तेलंगाना जैसे प्रभावित राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जहां यह संघर्ष विशेष रूप से तीव्र है। यहां अपतटीय पवन और रूफटॉप सोलर अन्यत्र हैं।
अधिक भूमि का उपयोग करके, बड़े पैमाने पर सौर परिनियोजन कुछ क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति को बदल सकता है। यदि पेड़ों और झाड़ियों को हटा दिया जाता है, तो सौर प्रतिष्ठान, वास्तव में, पौधों में पहले से संग्रहीत कार्बन की एक निश्चित मात्रा को छोड़ सकते हैं। बड़े सौर संयंत्र भी कुछ मामलों में वनीकरण के प्रयासों के रास्ते में आ सकते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये संयुक्त कारक, कार्बन की नेट रिलीज का कारण बन सकते हैं।
भारत में, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को अधिकांश, राज्य नियामक एजेंसियों द्वारा ‘हरित’ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश समय, निर्माण से पहले पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन करना अनिवार्य नहीं होता है। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नीति निरीक्षण, राज्यों को अक्षय विकास में भूमि के मुद्दों को कुशलतापूर्वक संबोधित करने से रोकता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग की योजना बनाते समय, बेहतर समन्वय की जरूरत है। साथ ही, अधिक मजबूत भूमि उपयोग लेखांकन, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के साथ सामने आने वाले ‘दो विपरीत वांछनीय स्थियों, गुणों अथवा वस्तुओं के बीच संतुलन बनाने’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
शहरी विकास के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण
शहर, किसी भी जलवायु शमन नीति के डिजाइन में रुचि का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि वे उत्सर्जन-गहन गतिविधि के केंद्र हैं। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। शहरों के भविष्य के आधे से अधिक निर्माण 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि देश के पास लो-कार्बन पाथवे विकसित करने का अनूठा अवसर है, जिसमें भवन और निर्माण, परिवहन, औद्योगिक, भूमि और बिजली क्षेत्र शामिल होंगे।
दिल्ली जैसे बेतरतीब फैले विशाल महानगरों के विपरीत, कॉम्पैक्ट शहरी डिजाइन, भूमि की खपत और पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली गिरावट को कम कर सकता है। भूमि की भारी खपत और पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट के पीछे प्रमुख कारण पेंड़ों का उखड़ जाना और जमीन का पक्का हो जाना है। यदि आवश्यक गतिविधियों वाले क्षेत्रों के बीच यात्रा दूरी को कम करने की योजना बनाई जाए तो अधिक कॉम्पैक्ट शहर परिवहन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। हालांकि, भारी कंक्रीट वाले, खराब वनस्पति वाले कॉम्पैक्ट शहरी क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव काफी हद तक बढ़ सकता है, जो आज कई भारतीय शहरों को प्रभावित करने वाली समस्या है। इससे ठंडी पैदा करने वाली ऊर्जा की जरूरत बढ़ेगी, जिससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ेगा।
इस मामले में, बेहतर तापीय गुणों वाली वैकल्पिक निर्माण सामग्री का उपयोग करने से कई लाभ हो सकते हैं। यह इनडोर कूलिंग मांगों को कम कर सकता है, बिजली की खपत को कम कर सकता है और संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है। एयर कंडीशनिंग का उपयोग कम होने से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन को कम कम करने में मदद मिलेगी। ठंडक पहुंचाने वाले उपकरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसों का इस्तेमाल होता है जो ग्रीनहाउस गैसें हैं। पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों को अपनाने से सीमेंट की मांग में कमी लाई जा सकती है जिससे अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक उत्सर्जन में भी कमी आ सकती है। सीमेंट के उत्पादन से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होता है। कुछ वैकल्पिक निर्माण सामग्री में फ्लाई ऐश, पेपर फाइबर और चावल की भूसी जैसे औद्योगिक और कृषि उप-उत्पादों का उपयोग किया जाता है। उनके उपयोग से सीमेंट की मांग कम हो सकती है और साथ ही अन्य छोटे पारिस्थितिक लाभ भी हो सकते हैं। इससे पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी, सीमेंट उत्पादन श्रृंखला का एक प्रमुख घटक, रेत खनन उद्योग पर दबाव से राहत मिल सकती है।
कम-कार्बन वाला नहीं है परिवहन के लिए जैव ईंधन
जब परिवहन की बात आती है, जैव ईंधन, पारंपरिक ईंधन के लिए ऊर्जा सुरक्षा और कम-कार्बन विकल्प प्रदान करते हैं। लेकिन जैव ईंधन को लेकर भारत की राष्ट्रीय नीति में वर्तमान में परिकल्पित सम्मिश्रण दरों (डीजल के लिए बायोडीजल का अनुपात) में विशेष रूप से इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त गन्ने की खेती की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह होगा कि खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि को जल-गहन गन्ने की खेती की ओर मोड़ना होगा। देश में सीमित व्यवहार्य जल संसाधनों के साथ, अधिक गन्ने की खेती से भी पानी की उपलब्धता पर गंभीर स्थानीय प्रभाव पड़ सकते हैं। यह बदले में भूजल निष्कर्षण में वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे पंपों की बढ़ती संख्या को बिजली देने के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होती है।
अंततः, प्रस्तावित ईंधन मिश्रणों के उपयोग से परिकल्पित उत्सर्जन बचत को अतिरिक्त गन्ना उत्पादन के विभिन्न प्रभावों से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रति संतुलित किया जा सकता है। यदि नीति को केवल परिवहन क्षेत्र के लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाए इन ‘अनपेक्षित परिणामों’ को कम किया जा सकता है गया है।
लंबी-अवधि के लक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं
ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो एक दीर्घकालिक रोडमैप की आवश्यकता को दर्शाते हैं जो किसी भी एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी की जटिलता को ध्यान में रखता है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत को केंद्र सरकार, राज्यों, उद्योगों और जनता के बीच अधिक प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण रूप से, लंबी-अवधि की रणनीतियों की घोषणा, जैसे, भारत का नेट-जीरो लक्ष्य, अल्पकालिक अवधि में विचलित नहीं होना चाहिए। इसके लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए। तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह की सहायता प्रदान करने के मामले में वैश्विक जिम्मेदारियां निभाई जानी चाहिए। पहले से घोषित डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं को लेकर निश्चिंत और संतुष्ट महसूस करना आसान है। लेकिन एक वास्तविक खतरा यह है कि उनके समर्थन के लिए ठोस रोडमैप के बिना, नेट-जीरो रणनीतियां केवल विलंब को प्रेरित कर सकती हैं जो तत्काल आवश्यक जलवायु कार्रवाई को स्थगित कर सकती हैं।
साभार:www.thethirdpole.net